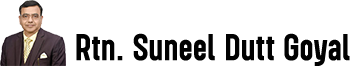R&D में निजी क्षेत्र को फ्री-हैंड: भारत की अगली छलांग का पासपोर्ट
भारत को अपनी अगली आर्थिक और रणनीतिक छलांग के लिए एक ही मंत्र चाहिए—निजी क्षेत्र को शोध और नवाचार में खुली छूट और बड़े प्रोत्साहन। आज भारत का कुल R&D निवेश जीडीपी के लगभग 0.5–0.7% के दायरे में अटका है, जबकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं 3.5–4.5% तक पहुंच चुकी हैं। चीन न सिर्फ अधिक निवेश करता है, बल्कि कंपनियों को 125–150% तक के सुपर-डिडक्शन, लंपसम कैश बोनस और पेटेंट खर्च का रीइम्बर्समेंट जैसी उदार नीतियां देकर निवेश को गुणा देता है—अर्थात यदि कोई कंपनी ₹100 करोड़ R&D में लगाती है तो कुल सरकारी सहायता का प्रभाव ₹250–₹300 करोड़ तक हो जाता है।
भारत को भी यही करना होगा: लागत घटाइए, जोखिम बांटिए, और निजी पूंजी को नवाचार की दौड़ में आगे बढ़ाइए। भारत को सूचना-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार-सर्विलांस/मॉनिटरिंग, रक्षा उत्पादन और मेडिकल-फार्मा R&D पर तत्काल प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी संप्रभुता और रोजगार सृजन के सबसे मजबूत इंजन बन सकते हैं ।
सूचना-प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)
भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को G20 स्तर पर परिभाषित और मान्यता दिलाई है, जिससे पहचान, भुगतान और डेटा-साझाकरण के माध्यम से समावेशी सेवा-प्रदायन का वैश्विक मानक स्थापित हुआ है । G20 टास्क फ़ोर्स की अंतिम रिपोर्ट बताती है कि DPI आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और शासन-परिवर्तन का आधार बन चुका है और इसे वैश्विक दक्षिण तक बढ़ाने का रोडमैप स्पष्ट है ।
दूरसंचार और सर्विलांस-मॉनिटरिंग
राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता के लिए स्पेस-आधारित सर्विलांस/रीकॉन और संचार अवसंरचना का तीव्र विस्तार आवश्यक है, जिसे आगामी 3 वर्षों में 100–150 अतिरिक्त उपग्रह जोड़कर सुरक्षा और मॉनिटरिंग क्षमताओं को मजबूत करने की योजना से बल मिलेगा । वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप ऊर्जा व रक्षा R&D पर सरकारी समर्थन तेज़ी से बढ़ रहा है, जो उन्नत दूरसंचार और स्पेस-आधारित मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में नवाचार को गति देने का अवसर है ।
रक्षा और साइबर: नई लड़ाइयों की तैयारी
भविष्य की लड़ाइयां “स्टार-वॉर” जैसी हाई-टेक वॉरफेयर होंगी—उपग्रहों, ड्रोन, AI, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर डोमेनों में। यूक्रेन-रूस युद्ध ने दिखाया कि ₹50,000 का ड्रोन ₹100 करोड़ के टैंक को निष्क्रिय कर सकता है; शक्ति का समीकरण तकनीक से तय होगा। चीन की कक्षा में सैकड़ों निगरानी उपग्रह सक्रिय हैं; भारत के पास निगरानी/रीकॉन क्षमता में विस्तार की भारी गुंजाइश है।
यदि हमारी परमाणु पनडुब्बी परियोजना 2038 तक पूरी होगी, तो यह प्रश्न जरूरी है: तब तक तकनीक कहां पहुंच चुकी होगी? उत्तर साफ है—हमें समय-संवेदी, निजी भागीदारी-आधारित मॉडल अपनाना होगा, जहां डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइपिंग तक निजी उद्योग और स्टार्टअप्स अग्रिम पंक्ति में हों, और सरकार एंकर-ग्राहक बने। साइबर सुरक्षा में भी निजी क्षेत्र को फ्री-हैंड, बड़े प्रोत्साहन और तेज़ अनुमतियां देकर रेड-टीमिंग, जीरो-ट्रस्ट, क्रिप्टोग्राफी, और सुरक्षा-ग्रेड हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर में तेजी लानी होगी। अगला युद्ध भौतिक सीमाओं से पहले फाइबर और स्पेक्ट्रम में लड़ा जाएगा।
फार्मा और मेडिकल R&D: लैब-ऑफ़-द-वर्ल्ड की ओर
भारत सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) में वैश्विक ताकत है और अमेरिका सहित कई देशों को भारी मात्रा में निर्यात करता है। यह लाभ उठाने का समय है—किडनी, लिवर, ब्रेन, स्पाइन, मानसिक स्वास्थ्य, डायबिटीज, कैंसर, बोन मैरो, थैलेसीमिया जैसे क्षेत्रों में मिशन-मोड R&D को बढ़ावा देकर क्लीनिकल-टेक, बायोसिमिलर्स, जीन-थेरेपी और मेडिकल-डिवाइस में वैश्विक लीड ली जा सकती है। IP जनरेशन, क्लिनिकल ट्रायल इकोसिस्टम, रेगुलेटरी फास्ट-ट्रैक और अस्पताल-उद्योग-अकादमिक गठजोड़ से भारत “फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड” से “लैब ऑफ द वर्ल्ड” बन सकता है।
AI-IT और इंडस्ट्रियल R&D: प्रतिभा है, नीति चाहिए
AI, सेमीकंडक्टर उप-प्रणालियां, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मटेरियल्स और ग्रीन-टेक में भारत के पास युवा प्रतिभा और IIT परिसरों से निकलती डीप-टेक कंपनियों का पूल है। बाधा है—उच्च पूंजी लागत, IP जोखिम, धीमी अनुमतियां और अनिश्चित मांग। सरकार यदि एंकर-ग्राहक बने, मानकीकरण और टेस्ट-बेड दे, और कर-प्रोत्साहन से लागत घटाए, तो निजी निवेश स्वतः बढ़ेगा। संक्षेप में, सरकार को दिशा और भरोसा देना है; पूंजी और क्रियान्वयन युवा कर देगा।
क्या करना होगा: एक साहसी प्रोत्साहन पैकेज
सुपर-डिडक्शन और कैश सपोर्ट: निजी R&D व्यय पर 150–200% सुपर-डिडक्शन; प्रोटोटाइप/TRL-लक्ष्य प्राप्ति पर लंपसम कैश बोनस; पेटेंट फाइलिंग/प्रोसीक्यूशन/विदेशी फाइलिंग फीस का 100% तक रीइम्बर्समेंट (सीलिंग के साथ)।
मैचिंग ग्रांट्स: ₹5–₹50 करोड़ तक मैचिंग-ग्रांट स्कीम, विशेषकर डीप-टेक/डिफेंस-टेक/बायो-टेक के लिए, जहां निजी पूंजी के साथ सरकार जोखिम साझा करे।
तेज़ अनुमतियां: डिफेंस और साइबर R&D के फील्ड-ट्रायल/इम्पोर्ट-लाइसेंस/एक्सपोर्ट NOC के लिए 30–90 दिन की टाइम-लिमिटेड, सिंगल-विंडो क्लियरेंस।
एंकर-प्रोक्योरमेंट: iDEX जैसे मॉडलों का विस्तार; “ट्रायल-टू-प्रोक्योर” फ्रेमवर्क ताकि सफल प्रोटोटाइप को तेज़ी से ऑर्डर मिलें; MSME/स्टार्टअप को कोटा।
IP कमर्शियलाइजेशन: सार्वजनिक लैब/PSU IP को स्टार्टअप्स हेतु रॉयल्टी-लाइट लाइसेंस; “सॉवरेन पेटेंट फंड” जो रणनीतिक पेटेंट खरीद/संरक्षण करे।
R&D वाउचर और टैक्स क्रेडिट: SMEs को प्रयोगशालाएं/टेस्ट-बेड उपयोग हेतु वाउचर; 10 वर्ष के लिए R&D टैक्स-क्रेडिट की स्थिरता ताकि प्लांट और प्रतिभा पर दीर्घकालीन निवेश हो।
त्वरित अवमूल्यन और Capex सपोर्ट: लैब उपकरण/क्लीन-रूम/टेस्ट-रिग पर 1–2 वर्ष में त्वरित अवमूल्यन; पूंजी-गहन डीप-टेक के लिए क्रेडिट गारंटी।
साइबर-टेक बूस्ट: राष्ट्रीय बग-बाउंटी/रेड-टीम कार्यक्रम; सरकार-उद्योग डेटा सैंडबॉक्स; सुरक्षा-ग्रेड ओपन-सोर्स के लिए अनुदान।
फार्मा-मिशन: रोग-विशेष मिशन (कैंसर, डायबिटीज, थैलेसीमिया, मानसिक स्वास्थ्य) के लिए स्तरित-ग्रांट, तेज़ नैतिक-स्वीकृतियां, और ग्लोबल ट्रायल नेटवर्क से कनेक्टिविटी।
टैलेंट और इन्क्यूबेशन: “एंटरप्रेन्योर-इन-रेज़िडेंस” फैलोशिप, शहर-स्तरीय डीप-टेक क्लस्टर, और विश्वविद्यालय-उद्योग संयुक्त लैब्स जिनके परिणामों की खरीद का पूर्व-प्रतिबद्ध रोडमैप हो।
शासन-सुधार: नीति की विश्वसनीयता ही पूंजी है
R&D निवेश का सबसे बड़ा मित्र नीति-स्थिरता है। 10-वर्षीय स्पष्ट रोडमैप, कर-नीति में उलटफेर से बचाव, मानकीकरण/टेस्टिंग ढांचे का आधुनिकीकरण, और डेटा/गोपनीयता/निर्यात नियमों की स्पष्टता—ये सब निजी जोखिम घटाते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की “समस्या-सूचियां” नियमित रूप से जारी हों ताकि स्टार्टअप्स सटीक समाधान विकसित करें। सबसे बढ़कर, सरकार अनुमोदक से सक्षमकर्ता बने—न्यूनतम फॉर्म, अधिकतम विश्वास, और परिणाम-आधारित जवाबदेही।
निष्कर्ष: नेतृत्व की नियति और युवा की ऊर्जा
भारत के उद्योगपति और युवा इंजीनियर-साइंटिस्ट में वह क्षमता है जो वैश्विक मानचित्र बदल सकती है। उन्हें सिर्फ अधिकार, भरोसा और प्रोत्साहन चाहिए। सरकार की पूंजी से अधिक मूल्यवान है सरकार का स्पष्ट संकेत: निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता, बड़े इंसेंटिव और तीव्र अनुमतियां मिलेंगी। यही समय है जब भारत लागत-प्रतिस्पर्धा से ज्ञान-प्रतिस्पर्धा की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए—वरना कल की लड़ाइयों में आज की हिचकिचाहट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी।
धन्यवाद,
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
suneelduttgoyal@gmail.com