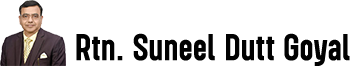देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि है। इसी स्मृति स्थल पर देश के कई शीर्ष नेताओं की समाधियां बनाई गई हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सभी प्रमुख नेताओं को यहां समान रूप से स्थान मिला है?
इस स्मृति स्थल पर भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की समाधि नहीं है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की समाधि भी यहां नहीं है। हालांकि, एक ही परिवार के चार सदस्यों—पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी—की समाधियां यहां मौजूद हैं। यह व्यवस्था यह संकेत देती है कि देश के लिए सबसे अधिक योगदान इसी परिवार का रहा है, जबकि अन्य नेताओं के योगदान को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर विवाद
हाल ही में, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने मांग उठाई कि उनकी समाधि स्मृति स्थल में बनाई जाए। सरकार ने उनकी समाधि बनाने पर सहमति जताई, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जगह पर नहीं। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर हुआ था, जिसके बाद उनके परिवार को स्मृति स्थल में समाधि के लिए स्थान चुनने का प्रस्ताव दिया गया।
क्या स्मृति स्थल में समाधि बनाने के लिए नैतिक मापदंड हैं?
यह विचारणीय प्रश्न है कि स्मृति स्थल पर किन नेताओं की समाधि होनी चाहिए? क्या ऐसे नेता, जिन्होंने जब भी अवसर आया, देश और परिवार के बीच चुनाव करते समय परिवार को प्राथमिकता दी, वहां समाधि के योग्य हैं? क्या ऐसे नेता, जिनके कार्यकाल में आतंकवादियों को निर्दोष घोषित किया गया, जिनके शासन में पाकिस्तान लगातार हमले करता रहा और मुंबई हमला जैसी घटनाएं हुईं, वहां समाधि पाने के हकदार हैं?
डॉ. मनमोहन सिंह का 10 वर्षों का कार्यकाल विभिन्न घोटालों और विवादों से भरा रहा। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कोयला घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, और कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे मामलों ने देश की राजनीति को हिला दिया था। उनके कार्यकाल में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए।
आर्थिक सुधारों के बावजूद आलोचनाएं
डॉ. मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन क्या यह उपलब्धि पूरी तरह से उनकी थी? 1991 में, जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। यह कहा जाता है कि नरसिंह राव ने सभी प्रमुख आर्थिक फैसले लिए, लेकिन पूरा श्रेय डॉ. मनमोहन सिंह को मिला।
इसके अलावा, 1990 में इंग्लैंड में हुई एक गुप्त बैठक में कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सुझाव दिया था कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाए। इस बैठक के बाद, भारत की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव आए, जिनमें विनिवेश, उदारीकरण और निजीकरण शामिल थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इन सुधारों के पीछे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का दबाव था, और मनमोहन सिंह केवल एक कार्यान्वयनकर्ता थे।
राजनीतिक असहायता और आत्मसम्मान की कमी
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई ऐसे उदाहरण सामने आए, जिनमें उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे। एक ऐसा प्रधानमंत्री, जो एक आतंकवादी यासीन मलिक—जिसके ऊपर भारतीय वायुसेना के तीन अधिकारियों की हत्या का मुकदमा चल रहा था—उसे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाता है, और खड़े होकर उससे हाथ मिलाकर गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है जैसे वो आतंकी कोई राष्ट्राध्यक्ष के समान हो। जब मैंने यह दृश्य टीवी और समाचार पत्रों में देखा, तो मेरा खून खौल उठा। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इतना निर्बल और निर्णयहीन प्रधानमंत्री हमारे देश का कैसे हो सकता है?
एक ऐसा प्रधानमंत्री, जिसे न अपनी गरिमा की परवाह थी और न ही अपने पद की प्रतिष्ठा का ख्याल। उनके कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक फैसले को उनकी ही पार्टी के एक सामान्य सांसद—श्री राहुल गांधी—ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया। यह घटना उस समय घटी जब डॉ. मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर थे, और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे देखा। यदि उनमें ज़रा भी आत्मसम्मान होता, तो उसी समय इस्तीफा दे देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए एक विशेष परिवार के प्रति निष्ठा और पद से चिपके रहने की भावना अधिक महत्वपूर्ण थी।
इस देश ने पहले कभी इतना बेबस और निर्णयविहीन प्रधानमंत्री नहीं देखा। ईश्वर से प्रार्थना है कि भविष्य में हमें फिर कभी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय न देखना पड़े।
एक ऐसा प्रधानमंत्री, जिनके 10 वर्षों के कार्यकाल में पाकिस्तान लगातार भारत पर हावी रहा। आए दिन बम धमाके, विस्फोट और आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहीं। कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चरम पर थे। लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री महोदय में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह कोई कठोर कदम उठाते—सामान्य प्रतिक्रिया देना तो दूर की बात थी।
दूसरी ओर, हमारा पड़ोसी देश चीन भी अपनी मनमर्जी करता रहा, सीमाओं पर अतिक्रमण करता रहा, और भारत की संप्रभुता को चुनौती देता रहा। दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति एक दशक तक भारत का प्रधानमंत्री रहा।
क्या स्मृति स्थल केवल एक परिवार के लिए आरक्षित है?
राजघाट पर स्मृति स्थल में समाधि बनाने की परंपरा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि यह स्थान राष्ट्रीय स्मारक है, तो क्या यह सभी प्रमुख नेताओं के लिए समान रूप से खुला नहीं होना चाहिए? क्यों सरदार पटेल, डॉ. अंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं को यह सम्मान नहीं दिया गया? और क्या घोटालों और विवादों से घिरे नेताओं को इस स्थान पर समाधि बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए?
यह प्रश्न केवल डॉ. मनमोहन सिंह के समाधि स्थल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में वंशवाद, पक्षपात और ऐतिहासिक भेदभाव की ओर भी इशारा करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म में पारंपरिक रूप से समाधि या कब्र के रूप में स्मारक बनाने की कोई अवधारणा नहीं रही है, जैसी कि ईसाई, यहूदी या इस्लाम धर्म में पाई जाती है। इस्लाम में भी सुन्नी मुसलमान आमतौर पर मज़ार नहीं बनाते। हिंदू धर्म में मृतकों का अंतिम संस्कार दाह क्रिया द्वारा किया जाता है, और उनकी राख को गंगा जैसी पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। ऐसे में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में स्मृति स्थलों की परंपरा को कुछ विशेष राजनैतिक परिवारों तक सीमित क्यों रखा गया है?
अब समय आ गया है कि सरकार इस पर विचार करे और स्मृति स्थल में समाधि के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष मापदंड स्थापित करे।
धन्यवाद,
सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जयपुर, राजस्थान
suneelduttgoyal@gmail.com