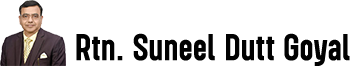भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपने हर नागरिक को मतदान का संवैधानिक अधिकार देता है। लेकिन जब यह अधिकार उन लोगों तक पहुंच जाए जो देश के नागरिक नहीं हैं — जैसे कि अवैध घुसपैठिए — तो यह लोकतंत्र की नींव को ही कमजोर कर देता है।
आज भारत इसी गम्भीर खतरे का सामना कर रहा है। विशेषकर सीमावर्ती राज्यों — पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश — में अवैध मतदाताओं की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ी है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
इस तकनीकी युग में चुनाव आयोग को चाहिए कि वह अपने सिस्टम में आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को शामिल करे, जिससे फर्जी या अवैध मतदाताओं की पहचान की जा सके और उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जा सके। डिजिटल KYC, आधार सत्यापन, और बॉयोमेट्रिक पहचान जैसे उपायों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ा जाना अब वक्त की मांग है।
यदि लोकतंत्र की सच्ची आत्मा को सुरक्षित रखना है, तो चुनाव आयोग को केवल प्रेक्षक या नियामक की भूमिका से आगे बढ़कर, सक्रिय सुधारक की भूमिका निभानी होगी।
चुनाव आयोग को आधुनिकरण की ज़रूरत है
पिछले 15 वर्षों में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद ज़रूरी सुधारों और बदलावों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया है। हर चुनाव—चाहे लोकसभा हो या विधानसभा या ग्राम सभा—के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट होती है। यह समझ से परे है कि अब तक एक सामान्य वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई है जो सभी स्तरों के चुनावों के लिए मान्य हो। मेरा पहला सुझाव यही है कि एक सामान्य जनरल वोटर लिस्ट बनाई जाए।
दूसरा अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिज़न्स) को घर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आधार पर वोटिंग की सुविधा देने का ट्रायल शुरू किया है। यह सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर देश से बाहर रहने वाले नागरिकों, दूसरे राज्यों में रह रहे कामकाजी लोगों या छात्र-छात्राओं को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती? उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक या पोस्टल माध्यम से वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए।
मैंने स्वयं लगभग एक साल पहले अपना वोटर आईडी ऑनलाइन अपडेट किया था, लेकिन आज तक वह मुझे नहीं मिला। इससे यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? इसे समय से आगे की सोच अपनानी होगी और तकनीकी रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा।
चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की सीमाएँ
एक और बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती तो कर देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि ज़िला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) और एसपी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। यह सही है कि आचार संहिता के समय वे आयोग के अंतर्गत होते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव प्रक्रिया में और गहराई तक की जाए, खासकर पोलिंग बूथ के अंदर।
अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जहां पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार के कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करते दिखते हैं। वोट किसे देना है, यह पूछते हैं और कई बार खुद वोट डाल देते हैं। यह अपने आप में एक नया “बूथ कैप्चरिंग” का तरीका है। इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल पोलिंग बूथ के अंदर तैनात हों और प्रत्येक वोटिंग प्रक्रिया पर निगरानी रखें। यहाँ हमारा यह सुझाव है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कहाँ और किस स्थान पर और कितनी होगी, यह भी चुनाव आयोग स्वयं अपने स्तर पर फैसला करें। तभी हम एक पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं।
आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो
आज हमारे पास ई-आधार, मोबाइल OTP, फेस आईडी और तमाम डिजिटल साधन मौजूद हैं। ऐसे में डाक द्वारा वोट भेजने की पुरानी प्रणाली को खत्म कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को विकसित करना चाहिए, ताकि जो लोग अपने गृह जनपद से बाहर हैं, वे भी आसानी से वोट डाल सकें।
जैसे चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारी तथा सीमा पर लगे हुए सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों में वे सभी अधिकारी जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर होते हैं, वे पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं। वैसे ही आम नागरिकों को भी दो दिन पहले वोट डालने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलनी चाहिए। यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है।
स्थानीय कारकों को समझे चुनाव आयोग
चुनाव आयोग को चाहिए कि वह अपने जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह जानकारी अवश्य प्राप्त करे कि उनके जिलों में मतदान के दिन या उससे एक-दो दिन पहले अथवा बाद में कोई बड़ा त्योहार, विवाह समारोह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजन तो नहीं है। यदि ऐसा कोई अवसर हो, तो ऐसी तारीखों से परहेज़ करते हुए वैकल्पिक मतदान तिथि का निर्धारण किया जाना चाहिए।
तारीख तय करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं वह दिन किसी और छुट्टी से न जुड़ जाए। आमतौर पर शनिवार और रविवार की छुट्टियां साथ लगने पर लोग ‘लॉन्ग वीकेंड’ मनाने चले जाते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में गिरावट आती है।
यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। यदि कोई नागरिक मतदान नहीं करता है, तो उसके लिए भविष्य में दंडात्मक प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है। यह भले ही आज के समय में असंभव सा लगे, लेकिन जब देश तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है, तो चुनाव आयोग का नवीनतम एवं सुदृढ़ और सुरक्षित तकनीक न अपनाना एक गंभीर चिंता का विषय है।
चुनाव आयोग को समय से आगे सोचते हुए कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता, चाहे वह देश में हो या विदेश में, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।
चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: सिर्फ नागरिकों को ही मिले वोट देने का अधिकार
हाल ही में नियुक्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव सुधारों की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने देशभर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे वैश्विक लोकतंत्रों की चुनावी प्रणाली और राज्य-स्तरीय चुनाव नियमों का गहन अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन सदन में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई-ऑफिस और डिजिटल फाइल मैनेजमेंट को भी लागू किया गया है — जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सराहनीय प्रयास हैं।
परंतु सवाल यह है कि क्या ये प्रयास मतदाता पहचान की शुद्धता को भी सुनिश्चित कर पाएंगे?
आज भारत के कई हिस्सों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध घुसपैठियों को वोटर आईडी जारी किए जा रहे हैं। इनमें से कई लोग न केवल मतदाता बन जाते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए ‘वोट बैंक’ में भी तब्दील हो जाते हैं।
दूसरा सवाल यह है कि इन दोनों चर्चाओं में आया है कि एक ही मतदाता के अलग-अलग जिलों में या शहरों में या राज्यों में कई वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इन डुप्लीकेट सिस्टम को जितनी शीघ्रता से चुनाव आयोग हटाएगा, उतना ही देश की सुरक्षा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए फायदेमंद होगा।
पश्चिम बंगाल: जनसांख्यिकीय बदलाव का जीवंत उदाहरण
पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दशकों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा से सटी ज़मीन पर हजारों लोग बगैर वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं और स्थानीय राजनैतिक समर्थन और ढीली प्रशासनिक जांच के कारण आसानी से भारतीय मतदाता बन जाते हैं।
यह जनसांख्यिकीय बदलाव न केवल स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गहराई से नुकसान पहुँचाता है। कई पूर्व अधिकारियों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में कुछ जगहों पर स्थानीय जनसंख्या में गैर-नागरिकों का अनुपात 25-30% तक पहुँच गया है।
चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों के पास वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ भी मौजूद होते हैं। चुनाव के समय इन वोटों का प्रयोग राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए होता है।
वोटर आईडी के लिए नागरिकता सत्यापन क्यों है ज़रूरी?
आज की प्रणाली में नाम, पता और उम्र के आधार पर वोटर आईडी मिल जाता है। कोई ठोस नागरिकता प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या नागरिकता पंजीकरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं है। नतीजतन, फर्जी पहचान पत्र बनाकर अवैध घुसपैठिये भी मतदाता बन जाते हैं।
इस घातक खामी को दूर करने के लिए निम्न उपाय अत्यंत आवश्यक हैं:
सभी नए और पुराने वोटर आईडी को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से जोड़ा जाए:
जिस तरह असम में NRC प्रक्रिया अपनाई गई, उसे तकनीकी रूप से दुरुस्त कर अब पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।
आधार, पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र से वोटर आईडी की क्रॉस वेरिफिकेशन:
आधार की बायोमेट्रिक जानकारी और पासपोर्ट की राष्ट्रीयता आधारित पुष्टि का उपयोग कर मतदाता पंजीकरण को अधिक सख्त बनाया जाए।
डिजिटल जियो-टैग्ड वेरिफिकेशन टीमों का गठन:
हर मतदाता के पते का ऑन-ग्राउंड डिजिटल सत्यापन किया जाए, जिससे फर्जी पते पर वोटर आईडी लेना मुश्किल हो।
फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान:
फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए सरकारी लाभ लेने या वोटर आईडी बनवाने पर कानूनी कार्रवाई हो और तुरंत आईडी निरस्त किया जाए।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ तभी संभव जब एक समान नागरिक पहचान सुनिश्चित हो
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की यह पहल कि पूरे देश में एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए — ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक — एक दूरदर्शी योजना है। लेकिन जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि इस सूची में केवल भारतीय नागरिक शामिल हों, तब तक यह प्रयास अधूरा और भ्रामक होगा।
राज्यों के बीच नियमों की असमानता, स्थानीय दबाव, भ्रष्टाचार और तकनीकी कमजोरियाँ मिलकर इस समस्या को और जटिल बना देते हैं।
निष्कर्ष: राष्ट्र की सुरक्षा और लोकतंत्र की शुचिता के लिए, चुनाव आयोग को नागरिकता सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी
भारत के सामने यह अब एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। जब घुसपैठिये मतदाता बनकर सत्ता के समीकरण तय करने लगें, तो यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मज़ाक बन जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के डिजिटल ट्रांजिशन प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि इन प्रयासों को मूलभूत पहचान सत्यापन के साथ जोड़ा जाए।
चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदाता पहचान और नागरिकता जाँच को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखे — क्योंकि बिना सच्चे नागरिकों के, लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा।
वे लोग जो अनपढ़ हैं या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे अक्सर चुनावी दलों और राजनेताओं के प्रभाव में आकर मतदान कर देते हैं। इस प्रकार, समाज के वही लोग—जो कि कम जानकारी रखते हैं—देश और प्रदेश की सत्ता का निर्धारण कर देते हैं, जबकि पढ़ा-लिखा वर्ग केवल तमाशबीन बना रहता है।
यह विडंबना है कि जो लोग देश और समाज को सही दिशा दे सकते हैं, वही अक्सर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। वे या तो आलस्यवश या छुट्टी का लाभ उठाने के लालच में मतदान से दूर रहते हैं। और जब गलत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तब वही लोग सबसे पहले शिकायत करते हैं। लेकिन वास्तव में, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं।
इसलिए मेरा देश के प्रत्येक नागरिक से विनम्र निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यह अधिकार केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके और आपके देश के साथ ही आपके बच्चों के भविष्य की नींव है। मतदान करते समय किसी के प्रभाव में न आएं, न ही किसी लालच में—बल्कि अपने विवेक और आत्मचिंतन के आधार पर सही उम्मीदवार को चुनें। एक जागरूक मतदाता ही एक उज्ज्वल भारत का निर्माण कर सकता है।
धन्यवाद,
सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष , जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
suneelduttgoyal@gmail.com