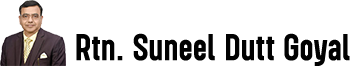एक ही व्यक्ति का दो सीटों पर चुनाव लड़ना कहाँ तक जायज़ है?
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर नागरिक को समान अधिकार के तहत वोट डालने और अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का हक़ मिला है। लेकिन समय-समय पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर जनता से लिया गया टैक्स आखिर खर्च कहाँ होता है? हाल के वर्षों में जिस मुद्दे ने बार-बार सुर्खियाँ बटोरी हैं, वह है — एक ही व्यक्ति का दो सीटों से चुनाव लड़ना।
दरअसल, आज “जनता की सेवा” शब्द नेताओं के लिए बदलकर “सत्ता प्राप्ति” और “कुर्सी बचाने” का खेल बन चुका है। नतीजा यह है कि कई बार सांसद या विधायक अपने वर्तमान पद या क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह चुनाव लड़ने चले जाते हैं। अगर जीत गए तो वहाँ चले जाते हैं, और हार गए तो पुरानी कुर्सी पर लौट आते हैं। सवाल यह है कि तब उस खाली हुई सीट का क्या? उस पर जब उपचुनाव होता है, तो उसका पूरा खर्च किसकी जेब से जाता है? जवाब साफ है — जनता का पैसा।
दो सीटों से चुनाव लड़ने का खेल
भारत में दो सीटों से चुनाव लड़ने की परंपरा कोई नई राजनीतिक चाल नहीं, इसकी जड़ें नेहरू-गांधी युग तक जाती हैं—और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों से लेकर आज तक कई बड़े नेताओं ने इसे रणनीतिक ढाल की तरह प्रयोग किया है । भारतीय चुनावी प्रणाली में अभी यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है। इसे पहली बार 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून (Representation of People Act) में अनुमति दी गई थी। तब तर्क यह दिया गया था कि किसी उम्मीदवार को अगर दो जगह से जनता का समर्थन चाहिए, तो उसमें बुराई नहीं। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह प्रावधान जनता के लिए मुसीबत और वित्तीय बोझ बन गया है। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में कांग्रेस का वर्चस्व था, और चुनावी ढाँचा आरपीए 1951 के तहत स्थापित हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को एक साथ एक से अधिक सीटों से नामांकन की अनुमति दी गई—यही प्रावधान आगे चलकर दो सीटों से लड़ने की वैधानिक आधारशिला बना ।
इंदिरा-राजीव से सोनिया-राहुल तक
कांग्रेस व्यवस्था के लंबे दौर में विपक्ष कमजोर होने के कारण बड़े नेताओं का “सुरक्षा” के रूप में एकाधिक सीटों से लड़ना समय के साथ अधिक दिखाई देने लगा। इंदिरा गांधी दो सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थीं—साल 1980 में उन्होंने रायबरेली (उत्तर प्रदेश) और मेडक (तब आंध्र प्रदेश) दोनों जगह से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीतीं; बाद में उन्होंने मेडक सीट छोड़ दी। 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी (कर्नाटक) और अमेठी (उत्तर प्रदेश) से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीतकर एक सीट छोड़ी—यही पैटर्न बाद के दशकों में भी बना रहा और उपचुनाव की बाध्यता सामने आती रही । 2019 में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से लड़े, वायनाड में जीते और अमेठी हारे—यह बताता है कि “डुअल कंटेस्ट” एक राजनीतिक जोखिम‑प्रबंधन उपकरण बना रहा, जिसका प्रभाव स्थानीय मतदाता पर और सार्वजनिक धन पर अलग‑अलग तरह से पड़ता है ।
यह भी देखा गया है की कई बार मौजूदा जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे देते हैं ताकि खाली हुई सीट पर उपचुनाव द्वारा किसी बड़े नेता को जितवा सकें. डी बी चंद्रे गौड़ा (D.B. Chandre Gowda) चिकमगलूर के मौजूदा कांग्रेसी सांसद थे, जो 1971 और 1977 में इस सीट से जीत चुके थे लेकिन 1978 में इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी के लिए पार्टी को एक “सुरक्षित सीट” की जरूरत थी इसीलिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, ताकि इंदिरा गांधी वहाँ से उपचुनाव लड़ सकें ।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है।
कुछ अन्य उदाहरण
ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसी कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं।
नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा में एकाधिक सीटों से नामांकन किए
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा, दोनों जगह से लड़े।
यानी यह एक आम राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। यह रणनीति केवल नेता का “सुरक्षा कवच” बनती है, मगर जनता की जेब और विश्वास पर भारी पड़ती है।
जनता का कितना पैसा डूबता है? (सरकारी आँकड़े)
भारत में चुनाव कराना बहुत महंगा कार्य है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:
2019 के लोकसभा चुनाव पर लगभग ₹60,000 करोड़ का खर्च हुआ था (जिसमें सरकारी और राजनीतिक पार्टियों का खर्च दोनों शामिल हैं)।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, एक लोकसभा उपचुनाव कराने का औसत खर्च 2–5 करोड़ रुपये होता है।
वहीं राज्य विधानसभा के उपचुनाव पर औसतन ₹1–2 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
अब जरा सोचिए — सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा नेता दो सीटों पर चुनाव लड़कर एक सीट खाली कर दे, जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या रोजगार योजनाओं में खर्च हो सकता था।
जनता के साथ अन्याय
यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक भी है। जब जनता वोट डालती है, तो वह उम्मीद करती है कि उसका प्रतिनिधि पूरे कार्यकाल तक उसकी सेवा करेगा। लेकिन जब प्रतिनिधि दूसरी जगह चला जाता है, तो उसी जनता को फिर से महीनों प्रचार, मतदान और चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
यानी एक तरफ जनता पर आर्थिक बोझ, और दूसरी तरफ जनता की राजनीतिक भावनाओं से खिलवाड़। क्या यह सीधे-सीधे विश्वासघात नहीं है?
समाधान क्या हो सकता है?
अब सवाल यह उठता है कि इसका व्यावहारिक समाधान क्या है?
1. दूसरे नंबर वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित करना
एक तर्क यह है कि अगर कोई नेता दो सीटों पर जीतता है और फिर एक सीट छोड़ देता है, तो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराने के बजाय रनर-अप (दूसरे स्थान पर आने वाले) को विजयी घोषित कर दिया जाए।
इससे करोड़ों रुपये बचेंगे।
नेता सोच-समझकर ही कई सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीट छोड़ते ही उनका विरोधी मजबूत होगा।
2. उपचुनाव का खर्च पार्टी या उम्मीदवार से वसूलना
अगर कोई प्रत्याशी सीट छोड़ता है, तो उस सीट के उपचुनाव का पूरा खर्च उसके या उसकी पार्टी से वसूला जाए। इससे उन्हें जनता के टैक्स की कीमत पता चलेगी।
3. केवल एक सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान
वैसे एक सबसे सीधा हल यह है कि कानून में संशोधन करके उम्मीदवार को केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।
1996 में भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजकर सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने दिया जाए।
लेकिन अब तक राजनीतिक दलों ने अपने हितों के चलते इस सिफारिश को लागू नहीं होने दिया।
अंतरराष्ट्रीय अनुभव
दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों ने पहले ही यह प्रथा खत्म कर दी है।
ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में उम्मीदवार एक समय में सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ सकता है।
बांग्लादेश जैसे देशों ने भी इस पर रोक लगा रखी है।
तो सवाल यह है कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के टैक्स के पैसे को ऐसे व्यर्थ बर्बाद करने की इजाज़त क्यों हो?
लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि
लोकतंत्र का मुख्य आधार यह है कि जनता सर्वोपरि है। नेताओं की व्यक्तिगत रणनीति या महत्वाकांक्षा जनता से बड़ी नहीं हो सकती। अगर एक सीट छोड़ने से करोड़ों रुपया बर्बाद होता है और जनता को दोबारा मतदान की मशक्कत करनी पड़ती है, तो यह साफ तौर पर अन्याय है।
आज जब देश विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असली मुद्दों से जूझ रहा है, तब चुनावी व्यवस्था को इतना महंगा और जटिल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यह वक्त है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर इस पर सख्त सुधार लाएँ।
अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो अपना वोट नहीं डाल सकता लेकिन वही कैदी भले ही दो साल से जेल में है तो वो चुनाव लड़ कर सांसद या विधायक बन सकता है. तो क्या वो जीता हुआ प्रत्याशी अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ न्याय कर रहा है ? उदाहरण के लिए, कश्मीर के बारामूला से सांसद शेख़ अब्दुल रशीद, जो इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है और तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद हैं ।
आम समझ से देखें तो जो व्यक्ति जनता की सेवा करने और मिलने‑जुलने के लिए “उपलब्ध” ही नहीं है, वह कैसे इलाके की समस्याएँ सुनेगा, जनसुनवाई करेगा या कामकाज देखेगा—जेल की दीवारें उसे लोगों से अलग कर देती हैं, और जनता उससे मिल भी नहीं पाती ।
इसी वजह से लोग कहते हैं कि यह लोकतंत्र का मज़ाक है: जनता तो वोट देने कतार में खड़ी रहती है, लेकिन लाखों लोग जो सिर्फ मुकदमे के चलते जेल में हैं, वोट नहीं डाल पाते, और दूसरी तरफ कोई बंदी कागज़ी औपचारिकताएँ पूरी करके चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है । बहुत से संगठनों और कानूनी बहसों में यह मांग उठी है जेल में रहने के दौरान चुनाव लड़ने पर साफ‑साफ रोक या सख्त शर्तें लगाई जाएँ, ताकि हक़ और ज़िम्मेदारी का संतुलन बना रहे और जनता का भरोसा कायम रहे ।
निष्कर्ष
आज जब हर परिवार महँगाई, बेरोजगारी और टैक्स के बोझ से दबा हुआ है, तब जनता का पैसा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर खर्च करना लोकतंत्र का मज़ाक है। अगर अनावश्यक उपचुनाव रोके जाएँ, तो करोड़ों रुपये का सदुपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे पर हो सकता है।
इसलिए अब वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग, संसद और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर बहस करे।
लोकतंत्र मज़बूत तभी होगा जब जनता का सम्मान रहेगा और उसके हित के विपरीत कोई नियम नहीं होगा। दो सीटों पर चुनाव लड़ना राजनीति का खेल नहीं, बल्कि जनता के साथ मज़ाक है — और इसको कानून बनाकर खत्म करना ही लोकतांत्रिक ईमानदारी की पहली शर्त है।
धन्यवाद,
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
suneelduttgoyal@gmail.com